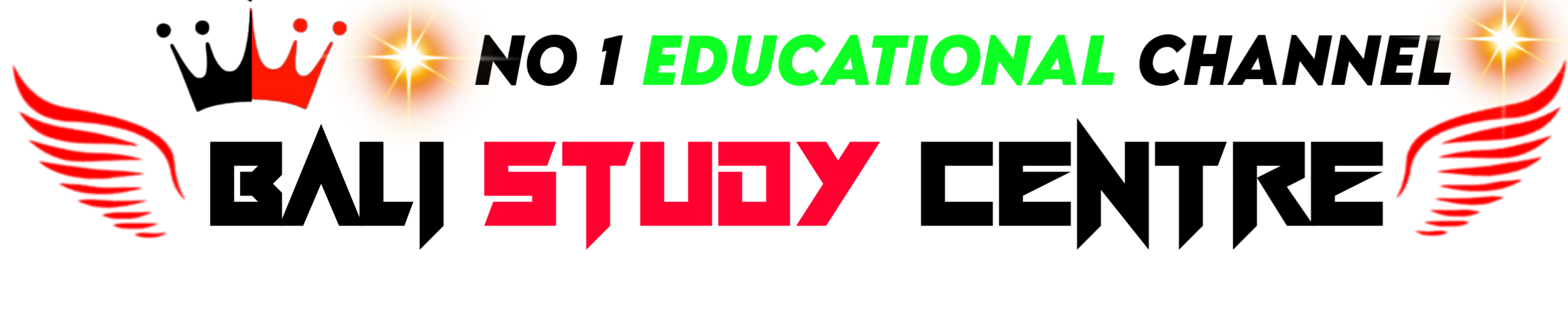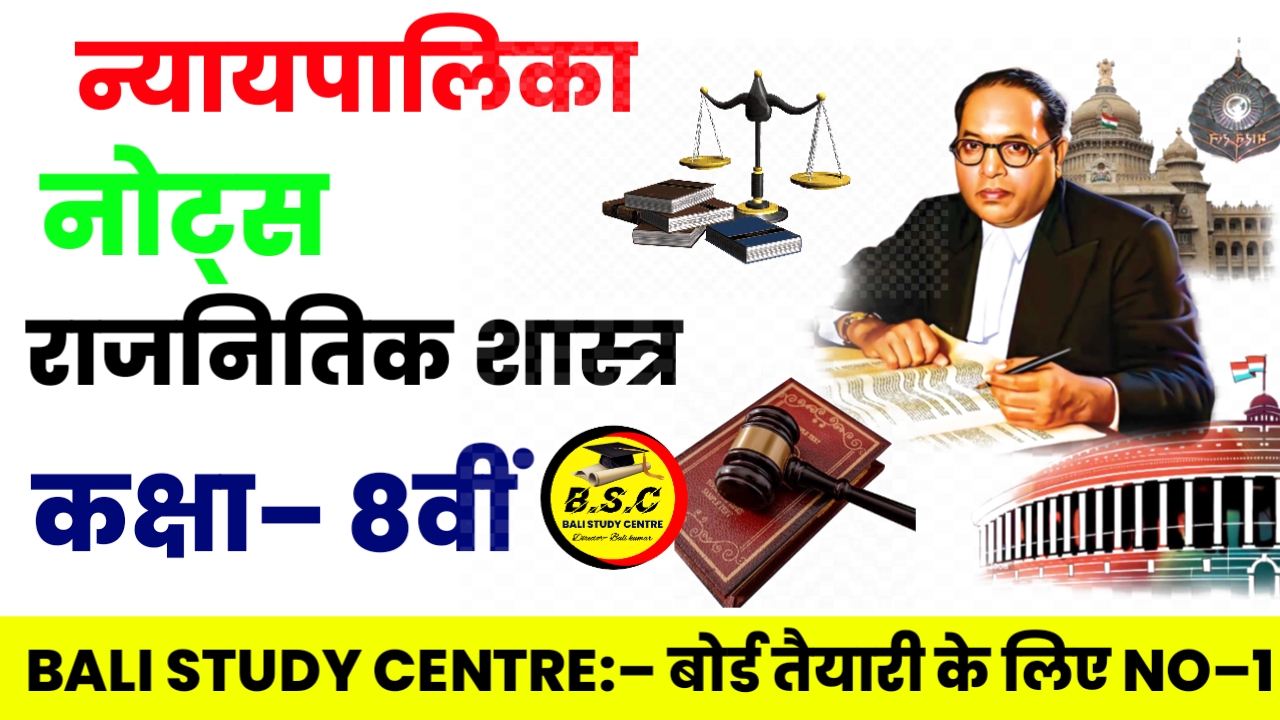आज के इस पोस्ट में हमलोग कक्षा 8वीं राजनीतिक शास्त्र का पाठ ‘न्यायपालिका’ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले है।
न्यायपालिका
👉 सरकार तीन अंगों द्वारा काम करती है।
(i) विधायिका— सरकार की वह शाखा जो कानून बनाने का काम करती है, उसे विधायिका कहते है।
(ii) कार्यपालिका— सरकार की वह शाखा जो कानून लागू करने का काम करती है, उसे कार्यपालिका कहते है।
(iii) न्यायपालिका— सरकार की वह शाखा जो बिना किसी पक्षपात या दबाव के किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने का कार्य करती है, उसे न्यायपालिका कहते है।
न्यायपालिका के मुख्य काम
(i) विवादों का निपटारा करना है। जैसे– नागरिकों के बीच झगड़े, नागरिक व सरकार के बीच झगड़े, दो राज्यों के बीच झगड़े, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच झगड़े।
(ii) न्यायिक समीक्षा करना = संविधान की व्याख्या करना और अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है, तो उसे रद्द करना है।
(iii) मौलिक अधिकारों की रक्षा = अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाए, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है।
26 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना हुई, उसी दिन भारत का गणतंत्र बना।
पहले सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था, लेकिन 1958 में यह अपनी नई इमारत में शिफ्ट हुआ।
स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि अदालतें सरकार या नेताओं के दबाव में काम नहीं करतीं है।वे बिना किसी डर या दबाव के निष्पक्ष फैसले सुनाती हैं। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो आम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा।
संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। सरकार की अन्य शाखाएँ (विधायिका और कार्यपालिका) अदालत के काम में दखल नहीं दे सकतीं है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है ताकि अदालतें सरकार या नेताओं की ग़लत हरकतों पर रोक लगा सकें। और नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जा सकें।
भारत में अदालतों की संरचना कैसी है?
भारत में तीन स्तर की अदालतें होती हैं।
(i) निचली अदालतें (जिला या तहसील स्तर की) = इन्हें अधीनस्थ या जिला अदालत कहते हैं। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है।
अधीनस्थ अदालतों को ट्रायल कोर्ट या ज़िला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है।
(ii) उच्च न्यायालय (High Court) = हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है। यह राज्य की सबसे ऊँची अदालत होती है।
(iii) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)= यह भारत की सबसे बड़ी अदालत है। यह नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं।
★ उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गयी, ये तीनों प्रेसिडेन्सी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। आज देशभर में 25 उच्च न्यायालय हैं।
पंजाब और हरियाणा का एक साझा न्यायालय है, जो चण्डीगढ़ में स्थित है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय। 2019 से आंध्र प्रदेश (अमरावती) और तेलंगाणा (हैदराबाद) में अलग-अलग उच्च न्यायालय हैं।
भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मानने होते हैं। अगर किसी को निचली अदालत का फैसला गलत लगे तो वह ऊँची अदालत में अपील कर सकता है।
लक्ष्मण कुमार केस — एक उदाहरण
1980 में लक्ष्मण कुमार ने सुधा गोयल से शादी की। 2 दिसंबर 1980 को सुधा जलकर मर गई। सुधा के परिवार ने अदालत में केस किया।
🔵 निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) का फैसला
पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने सुधा को जलते हुए देखा। सुधा ने कहा — उसकी सास शकुंतला ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और पति लक्ष्मण ने आग लगाई।
निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और भाई सुभाष को मौत की सजा (फाँसी) सुनाई।
🔵 उच्च न्यायालय में अपील
1983 में तीनों ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने कहा — यह दुर्घटना थी, स्टोव से आग लगी थी। इसलिए तीनों को बरी (छुड़ा) कर दिया।
🔵 महिला संगठनों की चिंता
1980 के दशक में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ़ आंदोलन कर रहे थे। उन्हें यह फैसला गलत लगा, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
🔵 सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी माँ को दोषी माना, लेकिन सुभाष को सबूत न मिलने के कारण बरी किया।सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और शकुंतला को उम्रकैद की सजा दी।
विधि व्यवस्था की दो मुख्य शाखाएँ
(i) फ़ौजदारी कानून (Criminal Law)
(ii) दीवानी कानून (Civil Law)
फौजदारी कानून उन मामलों से जुड़ा है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जैसे– चोरी, दहेज के लिए महिला को तंग करना, हत्या
प्रक्रिया
सबसे पहले एफ़.आई.आर. (FIR) दर्ज होती है।इसके बाद पुलिस जांच करती है। फिर अदालत में केस चलता है। दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना भी लग सकता है।
दीवानी कानून व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा होता है। जैसे– जमीन की खरीद-बिक्री का विवाद, किराए का झगड़ा, तलाक आदि
क्या हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है?
हाँ, भारत का हर नागरिक अदालत की शरण में जा सकता है। हर नागरिक को न्याय माँगने का अधिकार है। और अदालतें हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। अगर किसी को लगे कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह अदालत जा सकता है।
लेकिन गरीबों के लिए मुश्किल क्यों?
अदालत में जाने में काफी पैसा, बहुत कागज़ी कार्यवाही और बहुत समय लगता है। अगर कोई गरीब अनपढ़ है और उसका परिवार दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो उसके लिए अदालत में केस करना बहुत मुश्किल होता है।
इसी वजह से 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) की व्यवस्था शुरू की।इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके।
अब कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे लोगों की ओर से PIL दायर कर सकती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। PIL उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेजा गया पत्र या तार (टेलीग्राम) भी PIL माना जाता है।
PIL के जरिए बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। और बिहार में जो कैदी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में थे, उन्हें छुड़वाया गया। तथा सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील (दोपहर का भोजन) भी PIL की वजह से शुरू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में अदालत ने कहा कि भोजन का अधिकार भी शामिल है।
2001 में राजस्थान और उड़ीसा में सूखा पड़ा, लाखों लोगों को भोजन की भारी कमी हो गई।दूसरी तरफ़ सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे।और बहुत सारे गेहूँ चूहे खा गए थे।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की। याचिका में कहा गया कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में भोजन का अधिकार भी शामिल है। तब सरकार ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा – गोदाम तो अनाज से भरे हैं, इसलिए यह दलील गलत है। और भोजन देना राज्य की जिम्मेदारी है।
ओल्गा टेलिस केस (1985)
✅ ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के केस में अदालत ने कहा – जीवन का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। इसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। झुग्गी (झोपडी) वालों को हटाने से उनकी रोज़ी-रोटी छिन जाएगी, इसलिए जीवन का अधिकार भी छिन जाएगा। अदालत ने कहा – ये लोग पटरी या झुग्गी में इसलिए रहते हैं, क्योंकि उनके काम वहीं होते हैं।
अदालतें मुकदमे की सुनवाई में कई-कई साल लगा देती हैं। इसलिए कहा जाता है – इंसाफ में देरी मतलब इंसाफ का कत्ल।
हाशिमपुरा मामला — न्याय में देरी का उदाहरण
1987 में हाशिमपुरा में 43 मुसलमानों की हत्या हुई। उनके परिवार 31 साल तक न्याय के लिए लड़ते रहे। मुकदमा यूपी से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2002 में स्थानांतरित हुआ। 2007 तक सिर्फ तीन गवाहों के बयान हुए। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों को सजा दी।
JOIN NOW
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऊपर दिए गए कक्षा 8वीं के राजनीतिक शास्त्र के पाठ 05 न्यायपालिका का नोट्स और उसका प्रश्न को पढ़कर आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद !